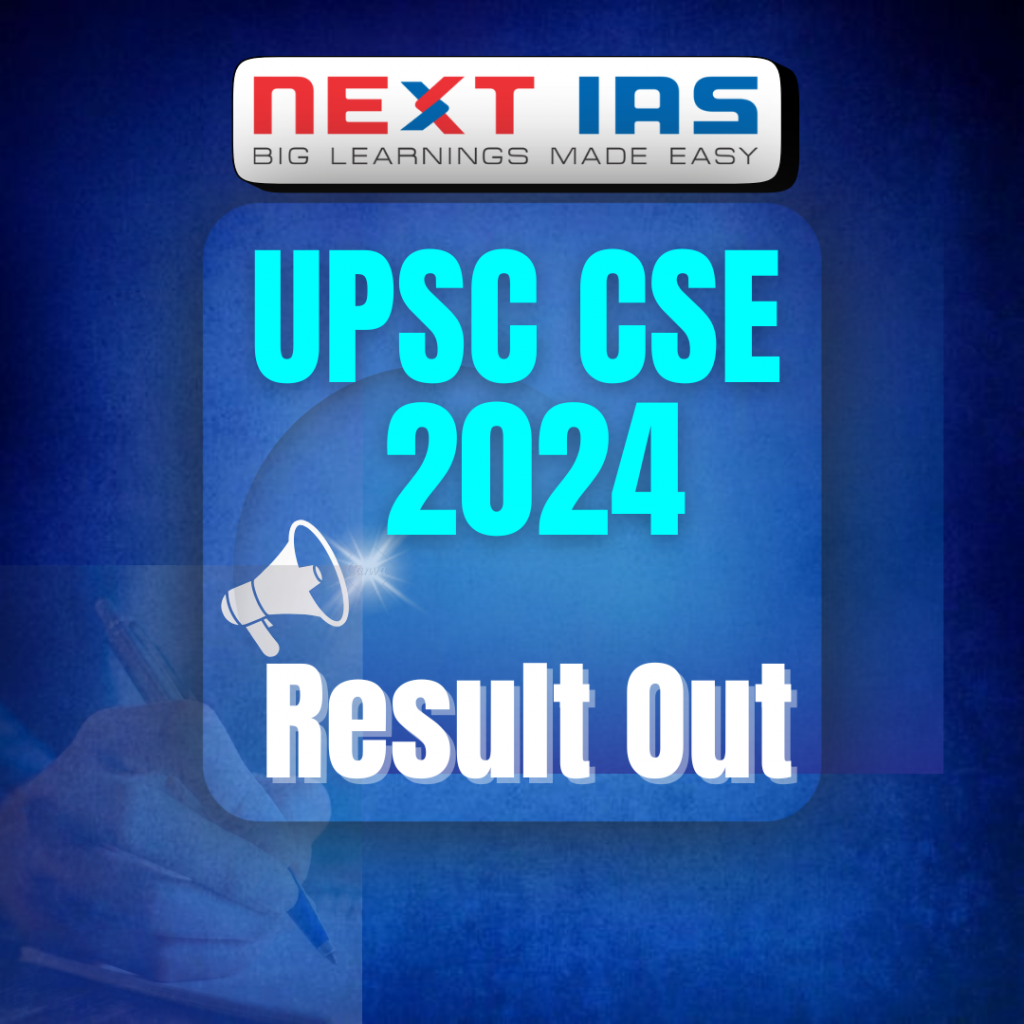भारत की विविध जलवायु और स्थलाकृति विभिन्न प्रकार के वनों प्रजातियों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक प्रकार के वन अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करते हैं। ये वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता का समर्थन करने और आवश्यक संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। इस लेख का उद्देश्य भारत में विभिन्न प्रकार के वनों, उनकी विशेषताओं, जलवायु परिस्थितियों और वितरण का विस्तार से अध्ययन करना है।
भारत में वनों के प्रकार
भारत की विविध जलवायु और स्थलाकृति विभिन्न प्रकार के वनों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक प्रकार के वन अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करते हैं। भारत में वनों के प्रकार मुख्य रूप से वर्षा, तापमान और ऊँचाई जैसे कारकों पर आधारित होते हैं। भारत की वनस्पति को पाँच मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:
- आद्र उष्णकटिबंधीय वन,
- शुष्क उष्णकटिबंधीय वन,
- पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन,
- पर्वतीय शीतोष्ण वन, और
- अल्पाइन वन।
इन सभी प्रकार के वनों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है।
आद्र उष्णकटिबंधीय वन
भारत में आद्र उष्णकटिबंधीय वनों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। जो इस प्रकार हैं:
उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन या वर्षा वन
- उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास के ऊपरी और निचले इलाकों में पाए जाते हैं।
- इन वनों में चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ों का वर्चस्व है, जो एक घने ऊपरी छत्र (पर्ण की परत) का निर्माण करते हैं। ये वन वनस्पति और अन्य जीवन की विविधता से भरपूर होते हैं।
- उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम (प्रमुख जीवन क्षेत्र) में से एक हैं।
भारत में वर्षा वनों की विशेषताएँ
- सदाबहार: ये वन उच्च गर्मी और आर्द्रता के कारण सदाबहार रहते हैं। पेड़ एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं।
- मेसोफाइटिक: ये पौधे न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत गीले जलवायु के अनुकूल होते हैं।
- सघन वितान : हवा से देखने पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पत्तियों की एक मोटी परत (वितान) की तरह दिखाई देते हैं।
- यह वितान केवल तभी टूटती है जब बड़ी नदियाँ इसे पार करती हैं या इसे खेती के लिए साफ किया जाता है।
- सभी पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए ऊपर बड़ते हुए आपस में संघर्ष करते हैं (ज्यादातर एपिफाइट्स—एक पौधा जो पेड़ या अन्य पौधे पर गैर-परजीवी रूप से बढ़ता है), जिसके परिणामस्वरूप एक अजीब परत व्यवस्था बन जाती है।
- ऊपर से देखने पर पूरी आकृति विज्ञान एक हरे कालीन की तरह दिखाई देती है।
- कम भूमिगत वनस्पति : घने जंगलों की मोटी कैनोपी सूर्य की किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोक देती है, जिससे भूमिगत वनस्पति कम उगती है। हालांकि, जो भूमिगत वनस्पति विकसित होती है, वह मुख्य रूप से बांस, फर्न, लता, ऑर्किड आदि जैसे छाया-सहिष्णु प्रजातियों से बनी होती है। ये पौधे कम रोशनी की परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं और पेड़ों की घनी कैनोपी से छनकर आने वाली प्रकाश में पनपते हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है, वार्षिक तापमान लगभग 25°- 27°C होता है, और औसत वार्षिक आर्द्रता 77% से अधिक होती है।
- शुष्क मौसम स्पष्ट रूप से कम अवधि का होता है।
वितरण
- इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग (समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर ऊपर), पूर्वांचल पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं।
लकड़ी
- इस प्रकार के वनों की लकड़ी बारीक दाने वाली, सख्त और टिकाऊ होती है, जिसे कठोर लकड़ी कहा जाता है।
- इनका वाणिज्यिक मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन घनी झाड़ियां, शुद्ध वृक्षों का अभाव तथा परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण इनका दोहन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।
- इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ महोगनी, मेसुआ, शीशम, सफ़ेद देवदार, कटहल, बेंत, बाँस आदि हैं।
भारत में उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन
- ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच संक्रमणकालीन वन हैं।
- ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की तुलना में अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
विशेषताएँ
- अर्ध-सदाबहार वन कम घने होते हैं। ये आद्र सदाबहार वनों की तुलना में अधिक समूहबद्ध (झुंडों या कॉलोनियों में पनपने वाले, सीधे खड़े) होते हैं। इन वनों की विशेषता है कि इनमें कई प्रजातियाँ होती हैं।
- पेड़ों के तनों पर आमतौर पर प्रचुर मात्रा में एपिफाइट्स (ऐसे पौधे जो पेड़ों या अन्य पौधों पर गैर-परजीवी रूप से बढ़ते हैं) पाए जाते हैं।
- महत्वपूर्ण प्रजातियों में पश्चिमी घाट में लॉरेल, शीशम, मेसुआ, और कांटेदार बाँस; हिमालयी क्षेत्र में सफेद देवदार, भारतीय शाहबलूत, चंपा, आम, आदि शामिल हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 200-250 सेमी होती है।
- औसत वार्षिक तापमान 24°C से 27°C के बीच होता है, और सापेक्ष आर्द्रता लगभग 75 प्रतिशत होती है।
- शुष्क मौसम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुकाबले उतना छोटा नहीं होता।
वितरण
- इस प्रकार के वन पश्चिमी तट, असम, पूर्वी हिमालय की निचली ढलानों, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में वितरित हैं।
लकड़ी
- उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तरह, ये वन कम घने होते हैं, इनमें अधिक शुद्ध स्टैंड होते हैं (जिसके कारण लकड़ी उद्योग यहाँ सदाबहार वनों की तुलना में बेहतर है), और इनमें दृढ़ लकड़ी पाई जाती है।
भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन
यह भारत में सबसे व्यापक प्रकार के वन होते हैं और इन्हें सामान्यतः मानसून वन कहा जाता है।
विशेषताएँ
- पेड़ अपनी पत्तियाँ वसंत और प्रारंभिक ग्रीष्मकाल के दौरान गिरा देते हैं, जब पर्याप्त आद्रता उपलब्ध नहीं रहती।
- इनका सामान्य रूप अत्यधिक गर्मी (अप्रैल-मई) में अनाच्छादित दिखाई देता है।
- उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में अनियमित शीर्ष मंजिल (25 से 60 मीटर) होती है।
- भारी रूप से उभरे हुए पेड़ और काफी हद तक पूरी तरह से उगी हुई झाड़ियाँ इन वनों की विशेषताएँ हैं।
- ये वन सदाबहार वनों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। हालाँकि, इन वनों के बड़े क्षेत्र खेती के लिए साफ़ किए जा चुके हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेमी होती है, और इन वनों का औसत वार्षिक तापमान लगभग 27°C होता है।
- औसत वार्षिक सापेक्ष आर्द्रता लगभग 60 से 75 प्रतिशत होती है। इन वनों में वसंत ऋतु (सर्दी और गर्मी के बीच) होती है और गर्मियों का मौसम शुष्क प्रकृति का होता है।
वितरण
- ये वन पश्चिमी घाट के आसपास सदाबहार वनों के बेल्ट के साथ चलने वाली पट्टी में पाए जाते हैं।
- ये तराई और भाबर क्षेत्र सहित शिवालिक पर्वतमाला के साथ 77° पूर्व से 88° पूर्व तक की पट्टी में भी पाए जाते हैं।
- इस प्रकार के वन मणिपुर और मिजोरम राज्यों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों, छोटा नागपुर पठार, ओडिशा के अधिकांश भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय रूप से वितरित हैं।
लकड़ी
- इन वनों में मुख्य प्रजातियाँ हैं- सागौन, साल, आँवला, बाँस, शीशम, चंदन और महुआ।
- अपनी उच्च स्तर की सामूहिकता (अधिक शुद्ध वन) के कारण, इस प्रकार के वनों का दोहन अपेक्षाकृत आसान है।
भारत में तटीय और दलदली वन
वे ताजे पानी और खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। खारा पानी समुद्री जल और नदियों के मुहाने में मौजूद ताजे पानी का मिश्रण होता है और इसकी लवणता 0.5 से 35 पीपीटी तक हो सकती है।
वितरण
- तटीय वन समुद्र तट के किनारे कई स्थानों पर पाए जाते हैं, जबकि दलदली वन केवल गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
- घने मैंग्रोव समुद्र तट के किनारे सुरक्षित नदियों के मुहाने, ज्वारीय खाड़ियों, बैकवाटर, नमक दलदलों और कीचड़युक्त भूमि में उगते हैं।
- वे लकड़ी के लिए मूल्यवान ईंधन प्रदान करते हैं। वे गंगा डेल्टा में सुंदरबन में सबसे अधिक स्पष्ट और घने हैं, जहां प्रमुख प्रजाति सुंदरी वृक्ष (Heritiera) है।
लकड़ी
- वे नाव बनाने के साथ-साथ निर्माण और भवन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं।
- इस प्रकार के वनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वृक्षों की प्रजातियाँ सुंदरी, अगर, राइज़ोफोरा, स्क्रू पाइन, बेंत और ताड़ आदि हैं।
शुष्क उष्णकटिबंधीय वन
भारत में शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों की विभिन्न श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं:
उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन
इस प्रकार के वनों को पूर्वी दक्कन शुष्क सदाबहार वन भी कहा जाता है, जो दक्षिण-पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है।
विशेषताएँ
- 12 मीटर तक ऊँचे छोटे कद के पेड़ मिलते हैं, जो विस्तृत कैनोपी के साथ फैले हुए होते हैं। हालाँकि, बांस और घास आदि यहाँ ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं।
- इस प्रकार के वनों के अंतर्गत आने वाली अधिकांश भूमि कृषि या कैसुरीना के बागानों के लिए साफ कर दी गई है।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है, जो मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच प्राप्त होती है।
- औसत वार्षिक तापमान लगभग 28°C होता है, जबकि औसत आर्द्रता लगभग 75% होती है।
वितरण
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में कैसुरीना सबसे लोकप्रिय कृषि वानिकी प्रजाति है।
लाभ
- यह वन प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। तटीय क्षेत्रों में रेखीय वृक्षारोपण (लाइन प्लांटिंग) से हवा की गति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- इस वनस्पति का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अपनी सजावटी उपस्थिति के कारण आकर्षक होता है। साथ ही यह उच्च गुणवत्ता वाली जलाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं।
- लकड़ी कागज के गूदे के लिए उपयुक्त होती है और लेखन, मुद्रण व लपेटने के कागज के निर्माण में एक उपयोगी कच्चा माल है। इनका औषधीय महत्व भी है जो इन्हें स्वास्थ्य के नजरिये से भी उपयोगी बनाता है।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
शुष्क पर्णपाती वन में अधिकांश पेड़ बढ़ते मौसम के अंत में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह सदाबहार वनों के विपरीत है, जहाँ अधिकांश पेड़ पूरे वर्ष “हरे” रहते हैं क्योंकि वे मौसमी रूप से नहीं बल्कि वर्ष के विभिन्न समय पर पत्ते गिराते हैं।
विशेषताएँ
- ये शुष्क पर्णपाती वन नम पर्णपाती वनों के समान होते हैं, लेकिन वे शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं।
- वे तुलनात्मक रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उग सकते हैं जो कि उनका मुख्य अंतर है।
- वे एक संक्रमणकालीन प्रकार के मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ नम पर्णपाती पेड़ गीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- इन वनों में बंद लेकिन असमान कैनोपी पाई जाती है। ये वन 20 मीटर तक ऊँचे पर्णपाती पेड़ों की मिश्रित प्रजातियों का घर होते हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
औसत वार्षिक वर्षा 100-150 सेंटीमीटर होती है।
वितरण
- वे राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिम बंगाल को छोड़कर हिमालय की तलहटी से कन्याकुमारी तक फैली एक अनियमित, चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं।
- महत्वपूर्ण प्रजातियाँ सागौन, मेपलवुड, शीशम, आम, बांस, लाल चंदन, लॉरेल, सैटिनवुड आदि हैं। इस जंगल के बड़े हिस्से को कृषि उद्देश्यों के लिए साफ कर दिया गया है। इस प्रकार के जंगल अत्यधिक चराई, आग आदि से पीड़ित हैं।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन
कांटेदार वन एक घनी झाड़ीदार वाला क्षेत्र है जिसमें मौसमी वर्षा के साथ शुष्क उपोष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों की वनस्पति विशेषताएँ पाई जाती हैं।
विशेषताएँ
पेड़ कम ऊंचाई के (अधिकतम 6 से 10 मीटर) और व्यापक रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। अकेशिया और यूफोरबिया आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारतीय जंगली खजूर आम है। कुछ घास आदि भी वर्षा ऋतु में उगती हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
औसत वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। आर्द्रता 50 प्रतिशत से कम होती है, और औसत तापमान 25°-30°C तक होता है।
वितरण
- वे राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, कच्छ और पड़ोसी सौराष्ट्र में पाए जाते हैं।
- यहाँ, वे थार रेगिस्तान में रेगिस्तानी प्रकार के जंगलों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के जंगल पश्चिमी घाट के किनारे भी उगते हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- महत्वपूर्ण प्रजातियाँ नीम, बबूल, कैक्टि आदि हैं।
भारत में पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन
भारत में पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वनों की विभिन्न श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं:
उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन
हिमालय के उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन एक पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो मध्य नेपाल की मध्य पहाड़ियों से दार्जिलिंग होते हुए भूटान और भारत तक फैले हुए हैं।
विशेषताएँ
- ये सदाबहार प्रजातियों के शानदार जंगल हैं। ये सदाबहार प्रजातियों के अपेक्षाकृत ऊँचे (20-30 मीटर) और घने जंगल हैं।
- आम तौर पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ सदाबहार ओक, चेस्टनट, ऐश, बीच, साल और पाइन हैं। पर्वतारोही और एपिफाइट भी आम तौर पर पाए जाते हैं।
- इस प्रकार के जंगल देश के दक्षिणी भागों में कम स्पष्ट हैं। ये केवल नीलगिरि और पलानी पहाड़ियों में समुद्र तल से 1070-1525 मीटर ऊपर पाए जाते हैं।
- यह एक “अवरुद्ध वर्षा वन” है जो वास्तविक उष्णकटिबंधीय सदाबहार से कम समृद्ध है। पश्चिमी घाट के उच्च भागों में वनों के उप-प्रकार मौजूद हैं, जैसे महाबलेश्वर, सतपुड़ा और मैकाल पर्वतमाला के शिखर, तथा अरावली पर्वतमाला में बस्तर और माउंट आबू के ऊंचे क्षेत्र।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 75 सेमी से 125 सेमी के मध्य होती है और औसत वार्षिक तापमान 18°-21°C तक पाया जाता है, जहाँ आर्द्रता लगभग 80 प्रतिशत तक होती है।
वितरण
- वे आम तौर पर पूर्वी हिमालय में, 88°E देशांतर के पूर्व में, 1000 से 2000 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं।
उपोष्णकटिबंधीय नम चीड़ के जंगल
यह पारिस्थितिकी क्षेत्र पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होते हुए नेपाल और भूटान तक एक लंबी, विच्छिन्न पट्टी के रूप में फैले हुए हैं।
विशेषताएँ
- आस-पास के चौड़े पत्तों वाले जंगलों की तुलना में, यह पारिस्थितिकी क्षेत्र न तो प्रजातियों में असाधारण रूप से समृद्ध है और न ही स्थानिकता में उच्च है।
- हालाँकि, इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के स्तनधारी शामिल हैं।
वितरण
- वे पश्चिमी हिमालय में 73°E और 88°E देशांतरों के बीच समुद्र तल से 1000 और 2000 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल्स और खासी हिल्स के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी उनकी उपस्थिति देखी जाती है।
लकड़ी
- चीड़ या चिल सबसे प्रमुख पेड़ है, जो सीधा ऊपर की और बड़ता है। यह फर्नीचर, बक्से और इमारतों के लिए मूल्यवान लकड़ी आदि प्रदान करता है।
- इसका उपयोग राल और तारपीन के उत्पादन के लिए भी किया जाता है।
उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन
- छोटे सदाबहार बौने पेड़ों और झाड़ियों वाला एक छोटा झाड़ीदार जंगल, जिसमें कांटेदार प्रजातियाँ, जड़ी-बूटियाँ और घास शामिल हैं। जैतून, बबूल मोडेस्टा और पिस्ता सबसे प्रमुख प्रजातियाँ हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 50-100 सेमी (दिसंबर-मार्च में 15 से 25 सेमी) है। गर्मियाँ पर्याप्त रूप से गर्म होती हैं, और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं।
वितरण
- यह भाबर, शिवालिक और पश्चिमी हिमालय में समुद्र तल से 1000 मीटर तक पाया जाता है।
पर्वतीय शीतोष्ण वन
पर्वतीय शीतोष्ण वनों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं:
पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन
- यह घने सदाबहार वन होते हैं। इनकी तनों की परिधि बड़ी होती है और शाखाएँ शैवाल, फर्न और अन्य एपिफाइट्स से ढकी होती हैं।
- पेड़ शायद ही कभी 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई प्राप्त करते हैं।
- देओदार, चिलौनी, भारतीय चेस्टनट, बर्च, प्लम, माचिलस, दारचीनी, लिटसिया, मैगनोलिया, नीला देवदार, ओक, हेमलॉक आदि प्रमुख प्रजातियाँ हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- यह 1800 से 3000 मीटर की ऊँचाई पर उगते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 150 सेमी से 300 सेमी के बीच होती है, जबकि औसत वार्षिक तापमान लगभग 11°C से 14°C होता है, और औसत आर्द्रता 80 प्रतिशत से अधिक होती है।
वितरण
वे तमिलनाडु और केरल की ऊँची पहाड़ियों और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
हिमालय के नम शीतोष्ण वन
- ये मुख्य रूप से शंकुधारी प्रजातियाँ होती हैं, जो प्रायः शुद्ध रूप में उगती हैं।
- पेड़ 30 से 50 मीटर ऊँचे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पेड़ देवदार, चीड़, सिल्वर फिर्स, स्प्रूस आदि हैं।
- ये उच्च और खुले जंगला के रूप में विकसित होते हैं, जिनमें झाड़ीदार अधिवृद्धि होती है, जिसमें ओक, रोडोडेंड्रोन और कुछ बांस शामिल होते हैं।
- ये वन निर्माण, लकड़ी और रेलवे स्लीपर के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी प्रदान करते हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- औसत वार्षिक वर्षा 150 सेमी से 250 सेमी तक होती है।
वितरण
- ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 1500 से 3300 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम में पूरे पर्वत श्रृंखला के दौरान फैले होते हैं।
भारत में हिमालयी शुष्क पर्वतीय वन
- इस प्रकार के वनों में शंकुधारी वनस्पति होती है, जिसमें ज़ेरोफाइटिक झाड़ियाँ होती हैं, जिनमें देवदार, ओक, राख, जैतून आदि मुख्य वृक्ष होते हैं।
जलवायु परिस्थितियाँ
- यहाँ वर्षा 100 सेमी से कम होती है और यह मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है।
वितरण
- इस प्रकार के वन हिमालय की आंतरिक शुष्क श्रेणियों में पाए जाते हैं, जहाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून बहुत कमज़ोर होता है। ये क्षेत्र लद्दाख, लाहुल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल और सिक्किम में हैं।
भारत में आलपाइन वन
- आलपाइन वनों की ऊँचाई 2900 से 3500 मीटर के बीच होती है। इन्हें उप-आलपाइन, आद्र आलपाइन झाड़ी और शुष्क आलपाइन झाड़ी में विभाजित किया जा सकता है। उप-आलपाइन वन आलपाइन झाड़ी और घास के मैदानों में पाए जाते हैं।
- ये शंकुधारी और चौड़े पत्ते वाले पेड़ों का मिश्रण होते हैं, जिसमें शंकुधारी पेड़ लगभग 30 मीटर तक और चौड़े पत्ते वाले पेड़ केवल 10 मीटर तक बढ़ते हैं।
- प्रमुख प्रजातियाँ देवदार, स्प्रूस, रोडोडेंड्रोन आदि हैं।
- आद्र अल्पाइन झाड़ी रोडोडेंड्रोन, बर्च आदि की एक कम सदाबहार घनी वृद्धि है, जो 3,000 मीटर की ऊँचाई पर विकसित होती हुई बर्फ की रेखा की सीमा तक फैली होती है।
- शुष्क अल्पाइन झाड़ी शुष्क क्षेत्र में समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली झाड़ीदार ज़ेरोफाइटिक बौनी झाड़ियों की सबसे ऊपरी सीमा है।
- जुनिपर, हनीसकल, आर्टेमीसिया आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं।
भारत में विभिन्न प्रकार के वनों की हिस्सेदारी
| वनों के प्रकार | कुल वन क्षेत्र (%) |
| उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती | 37 |
| उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती | 28 |
| उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार वन | 8 |
| पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र (चीड़) | 6.6 |
| उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन | 4 |
| पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन | 3.6 |
| अल्पाइन वन | 2.1 |
| तटीय और दलदली वन | 0.6 |
निष्कर्ष
भारत में वनों के प्रकार देश की पारिस्थितिक विविधता के प्रमाण हैं, जो अलग-अलग जलवायु और भौगोलिक कारकों द्वारा आकार लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार वनों से लेकर अल्पाइन झाड़ियों तक प्रत्येक वन प्रकार, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, वन्यजीवों का समर्थन करने और आवश्यक संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरक्षण प्रयासों को इन विविध वन पारिस्थितिकी प्रणालियों को उनके पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। इस प्रकार के वनों की विशेषताओं और वितरण को समझकर, हम उनके महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं?
भारत में अपनी जलवायु और स्थलाकृति के कारण विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और मैंग्रोव वन आदि।
भारत में 5 प्रकार के वन कौन से हैं?
भारत में 5 प्रकार के वन हैं:
– उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
– उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
– उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन,
– पर्वतीय वन, और
– मैंग्रोव वन।