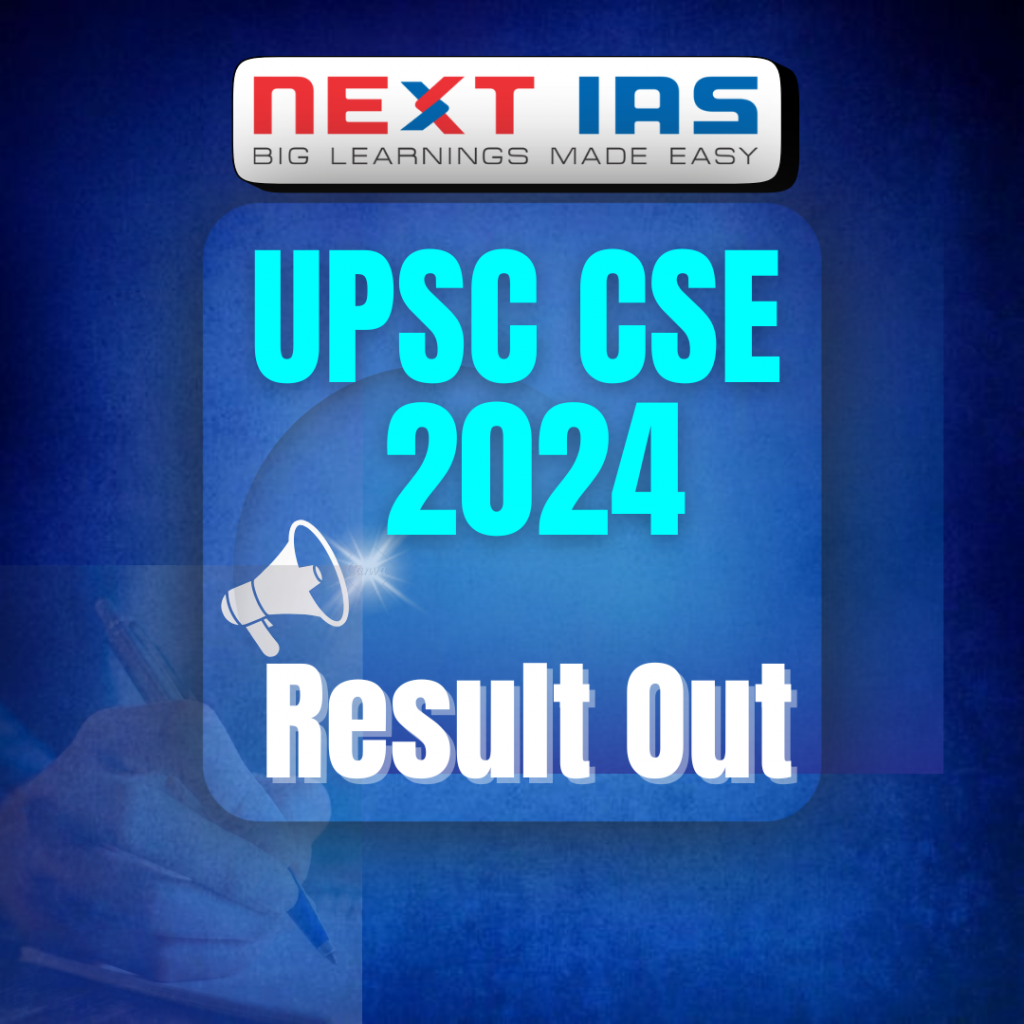भारत की सिंचाई प्रणाली इसके कृषि क्षेत्र की रीढ़ है, जो खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली का महत्व अविश्वसनीय मानसून वर्षा से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने, निरंतर कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता में निहित है। इस लेख का उद्देश्य भारत में सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करना है, जिसमें इसके भौगोलिक कारक, आवश्यकता, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और इसके विकास से जुड़ी चुनौतियाँ और समाधान शामिल हैं।
सिंचाई प्रणाली के बारे में
- सिंचाई कृषि की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव निर्मित प्रणालियों के माध्यम से पानी का नियंत्रित अनुप्रयोग है।
- सिंचाई, फसलों या पौधों को कृत्रिम पानी का अनुप्रयोग है, खासकर जब बारिश कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी प्रदान नहीं कर पाती है।
- दुनिया में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र होने के बावजूद, भारत में पानी की भारी कमी है। हमें सिंचाई के ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो ताजे पानी को बचाने में मदद करें और पौधों के विकास के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करें।
- इस प्रकार सिंचाई नदियों, तालाबों या भूमिगत जल जैसे स्रोतों से नहरों, कुओं, नलकूप, टैंकों आदि जैसे कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को पानी की आपूर्ति करती है।
- सिंचाई प्रणालियों के पीछे मुख्य विचार आवश्यक जल की न्यूनतम मात्रा बनाए रखते हुए फसलों और पौधों की वृद्धि में सहायता करना, अनाज के खेतों में खरपतवार की वृद्धि को रोकना और मिट्टी के जमाव को रोकना है।
- भारत में, कुल फसल क्षेत्र के दो-तिहाई हिस्से को सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में मानसून की वर्षा की प्रकृति अनिश्चित, अविश्वसनीय, अनियमित, परिवर्तनशील, मौसमी और असमान रूप से वितरित है।
विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के पक्ष में भौगोलिक कारक
उत्तरी मैदान
- भूमि की ढलान कम है जिससे नहरें सिंचाई के पानी को दूर-दूर तक ले जा सकती हैं।
- नरम और भुरभुरी मिट्टी के कारण नहरें और लिंक कुएँ खोदना आसान हो जाता है।
- उप-मृदा में गहरी मिट्टी वर्षा जल के लिए एक भंडार है, जो एक छिद्रपूर्ण माध्यम से रिसता है।
- इसलिए, कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई के लिए बड़ा भूजल उपलब्ध है।
प्रायद्वीपीय पठार
प्रायद्वीपीय पठार में सिंचाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति कठिन है तथा इसके लिए नीचे दिए गए कारक जिम्मेदार हैं:
- चट्टानें कठोर हैं, इसलिए नहरों और कुओं को खोदने में अधिक मेहनत लगती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से टैंक सिंचाई का अभ्यास किया जाता है।
- सतह असमान है, इसलिए नहरें दूर-दूर तक पानी ले जाने में असमर्थ सिद्ध होती हैं।
भारतीय कृषि में सिंचाई की आवश्यकता
मानसून की विशेषताएँ और भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव, जो सिंचाई को आवश्यक बनाता है, निम्नलिखित हैं:
- वर्षा का असमान वितरण- मानसून का आगमन अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, खासकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (परिवर्तनशीलता का उच्च गुणांक)।
- वर्षा के स्थानिक वितरण में भी भिन्नता होती है; उदाहरण के लिए, मेघालय में थार रेगिस्तान की तुलना में बहुत अधिक वर्षा होती है।
- अपर्याप्त कवरेज– केवल 30% खेती योग्य भूमि पर 100 सेमी से अधिक की पर्याप्त वर्षा होती है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, कृषि उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए सिंचाई आवश्यक है।
- मानसून में अंतराल (धूप वाले मौसम में दो या अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना) सिंचाई सुविधाओं के बिना फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- मौसमी प्रकृति– मानसून “मौसमी” है। वर्ष के 3-4 महीनों में 75% वर्षा होती है, और शेष 8-9 महीने शुष्क मौसम के होते हैं जब फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है (जैसे कि केरल में 5 महीने शुष्क होते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में नौ महीने शुष्क होते हैं )।
- वर्षा का प्रकार– भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा मूसलधार होती है, जिसके कारण मिट्टी के पास पानी को अवशोषित करने का कम अवसर होता है और सतही पानी व्यर्थ चला जाता है।
- इसके अलावा, पहाड़ी ढलानों के साथ वर्षा का पानी बहुत तेजी से बह जाता है। कुछ फसलें, जैसे चावल, गन्ना, जूट और कपास आदि को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इनकी सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
- मोनोकल्चर की समस्या– भारतीय कृषि में मोनोकल्चर फसल पद्धतियों को समाप्त करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। कृषि को परिवर्तनशील बनाकर ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए भी यह आवश्यक है।
- हरित क्रांति – ग्रीन क्रांति के बाद, HYV बीजों (उच्च उत्पादकता वाले बीज) और भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने सिंचाई को अधिक आवश्यक बना दिया है। जैसे कि बलुई और दोमट मिट्टी, जलोढ़ और काली मिट्टी की तरह पानी को रोककर नहीं रख सकती।
- बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक गहन कृषि होने लगी है, जिसके लिए अधिक सिंचाई सुविधाओं तथा अन्य इनपुट आदि की आवश्यकता होती है।
- पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी प्रदान करने, जिसमें महत्वपूर्ण पदार्थों का परिवहन शामिल है, सिंचाई आवश्यक होती है।
सिंचाई विकास का प्रभाव
- सिंचाई प्रणालियों के विकास ने फसलों के लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करके भारत में कृषि उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई है और खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, इसने मानसून की बारिश पर निर्भरता को कम करके, विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की आजीविका को स्थिर करने में मदद की है।
सिंचाई विकास के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है।
सिंचाई विकास के पर्यावरणीय प्रभाव
- सिंचित भूमि पर उत्पादन के लिए भूमि के नष्ट होने का प्रमुख कारण लवणीकरण है और यह सिंचाई से जुड़े सबसे अधिक प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों में से एक है।
- मिट्टी का जलभराव और लवणीकरण सतही सिंचाई से जुड़ी आम समस्याएँ हैं।
- जलभराव मुख्य रूप से अपर्याप्त जल निकासी और अत्यधिक सिंचाई के साथ साथ कुछ हद तक नहरों और खाइयों से रिसाव के कारण होता है।
- जलभराव मिट्टी की निचली परत से खींचे गए लवणों को पौधों के जड़ क्षेत्र में केंद्रित करता है।
- क्षारीयता, मिट्टी में सोडियम का निर्माण, लवणीकरण का एक विशेष रूप से हानिकारक रूप है जिसे सुधारना मुश्किल है।
- जल जनित या जल से संबंधित बीमारियाँ आमतौर पर सिंचाई की शुरूआत से जुड़ी होती हैं।
- सिंचाई से सीधे तौर पर जुड़ी बीमारियाँ मलेरिया आदि हैं, जिसके रोगवाहक सिंचाई के पानी में बढ़ जाते हैं।
- सिंचाई से संबंधित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों में कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते दबाव से जुड़े जोखिम शामिल हैं।
सिंचाई योजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- बड़े बांध निर्माण से उत्पन्न होने वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाढ़ की वजह से विस्थापित लोगों का पुनर्वास है।
- यह विशेष रूप से समुदायों के लिए विघटनकारी हो सकता है, और असंवेदनशील परियोजना विकास प्रभावित जनसंख्या के लिए अपर्याप्त मुआवजे के कारण अनावश्यक समस्याएं पैदा करेगा।
- मानव प्रवासन और विस्थापन समुदाय के बुनियादी ढांचे के टूटने के अनुरूप होते हैं, जिससे सामाजिक अशांति का स्तर बढ़ता है और यह कुपोषण में योगदान कर सकता है।
सिंचाई से जुड़ी समस्याएँ और चुनौतियाँ
- महंगी सूक्ष्म सिंचाई- इसे अपनाने वाले ज़्यादातर लोग अमीर हैं और गरीब किसान इसे वहन नहीं कर सकते। हालाँकि, विभिन्न एजेंसियों ने कम लागत वाली प्रणालियों का आविष्कार करके इस समस्या का समाधान किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्यम (IDE), एक गैर सरकारी संगठन, कम लागत वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का आविष्कार करने और गरीब किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
- परियोजनाओं के पूरा होने में देरी- पहली पंचवर्षीय योजना से ही हमारे प्रमुख और मध्यम सिंचाई क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या अधिक से अधिक नई परियोजनाएँ शुरू करने की प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं का प्रसार हुआ है।
- पहले से मौजूद संभावनाओं का उपयोग करने में भी देरी होती है। अधिकांश परियोजनाओं में, फ़ील्ड चैनल और जलमार्गों के निर्माण, भूमि समतलीकरण और भूमि को आकार देने में देरी हुई है।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद- भारत में सिंचाई राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से जल संसाधनों के विकास की योजना बनाते हैं।
- हालाँकि, सभी प्रमुख नदियाँ अंतर्राज्यीय प्रकृति की हैं। परिणामस्वरूप, भंडारण, प्राथमिकताओं और जल उपयोग के मामले में राज्यों में मतभेद हैं।
- संकीर्ण क्षेत्रीय दृष्टिकोण जल आपूर्ति के वितरण पर अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है।
- सिंचाई विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ- नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में अनुमान लगाया गया है कि प्रमुख, मध्यम और लघु योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधन विकास केवल 28.6 प्रतिशत है।
- इसके विपरीत, यह उत्तरी क्षेत्र में लगभग 95.3 प्रतिशत तक पहुँच गया है। यह सिंचाई सुविधाओं के विकास में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाता है।
- जलभराव और लवणता- सिंचाई की शुरूआत ने कुछ राज्यों में जलभराव और लवणता को जन्म दिया है, जिससे कृषि क्षेत्रों में नमक के तालाब बन गए हैं।
- सिंचाई की बढ़ती लागत– पहले पाँच वर्षों से लेकर अब तक सिंचाई प्रदान करने की लागत में वृद्धि हुई है।
- जल स्तर में गिरावट- देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, भूजल के अत्यधिक दोहन और वर्षा जल से अपर्याप्त पुनर्भरण के कारण हाल के वर्षों में जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।
- ग्रामीण और शहरी भारत में बिजली कटौती और अनिर्धारित रुकावटों के कारण ऊर्जा संकट- इस समस्या का समाधान ड्रिप सिंचाई को सोलर पैनल सिस्टम के साथ एकीकृत करके किया जा सकता है, जिसे ऑफ-ग्रिड किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। पीएम कुसुम योजना इस समस्या को कम करने के लिए की गई पहलों में से एक है।
सिंचाई परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के विकल्प
सिंचाई विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विकल्प मौजूद हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:
- सिंचाई परियोजना को उस स्थान पर स्थापित करना जहाँ नकारात्मक प्रभाव कम से कम हों।
- मौजूदा परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना और नई सिंचाई परियोजना स्थापित करने के बजाय उपयोग के लिए खराब हो चुकी फसल भूमि को बहाल करना।
- बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक स्वामित्व वाली और प्रबंधित योजनाओं के विकल्प के रूप में छोटे पैमाने पर, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सिंचाई प्रणाली विकसित करना।
- जलभराव, कटाव और अकुशल जल उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- जहां उपयुक्त हो, अन्य उपयोगकर्ताओं को अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए अपशिष्ट जल का उपचार करें।
- बांधों के नीचे बाढ़ प्रवाह को बनाए रखना आवश्यक है ताकि हर साल पर्याप्त क्षेत्र में बाढ़ आ सके, जिसमें मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए अन्य कारण भी शामिल हैं।
भारत में सिंचाई योजनाएँ
भारत में प्रमुख सिंचाई योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
- पीएमकेएसवाई का लक्ष्य देश के सभी कृषि फार्मों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ पैदा हो सके, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके।
- पीएमकेएसवाई की रणनीति सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम-से-अंतिम समाधान पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई है, जैसे कि जल स्रोत, वितरण नेटवर्क, कुशल खेत-स्तरीय अनुप्रयोग, नई तकनीकों और सूचनाओं पर विस्तार सेवाएँ आदि, जो जिला/राज्य स्तर पर एक व्यापक नियोजन प्रक्रिया पर आधारित हैं।
- जुलाई 2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री की पहल का उद्देश्य हर खेत के लिए सिंचाई (हर खेत को पानी) और उत्पादकता में वृद्धि (प्रति बूंद, अधिक फसल) सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक
- पीएमकेएसवाई के तीन केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के अंतर्गत चार घटक हैं।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) – जल शक्ति मंत्रालय।
- हर खेत को पानी (CADWM, RRR और लघु सिंचाई) – जल शक्ति मंत्रालय।
- प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय।
- वाटरशेड विकास (IWMP और MGNREGS)- ग्रामीण विकास मंत्रालय।
मिशन काकतीय
- मिशन काकतीय तालाबों और टैंकों जैसे लघु जल सिंचाई स्रोतों को बहाल करने के लिए तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास को बढ़ाना, विकेंद्रीकृत तरीके से समुदाय-आधारित सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करना और गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन के तहत लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटित 265 टीएमसी पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए टैंकों और जल स्रोतों की बहाली के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना है।
निष्कर्ष
भारत में सिंचाई प्रणालियों का विकास और प्रबंधन कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास और लाखों किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। सतत सिंचाई पद्धतियों को प्राथमिकता देकर भारत कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है, ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित कर सकता है और साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है।
सामान्य अध्ययन-1